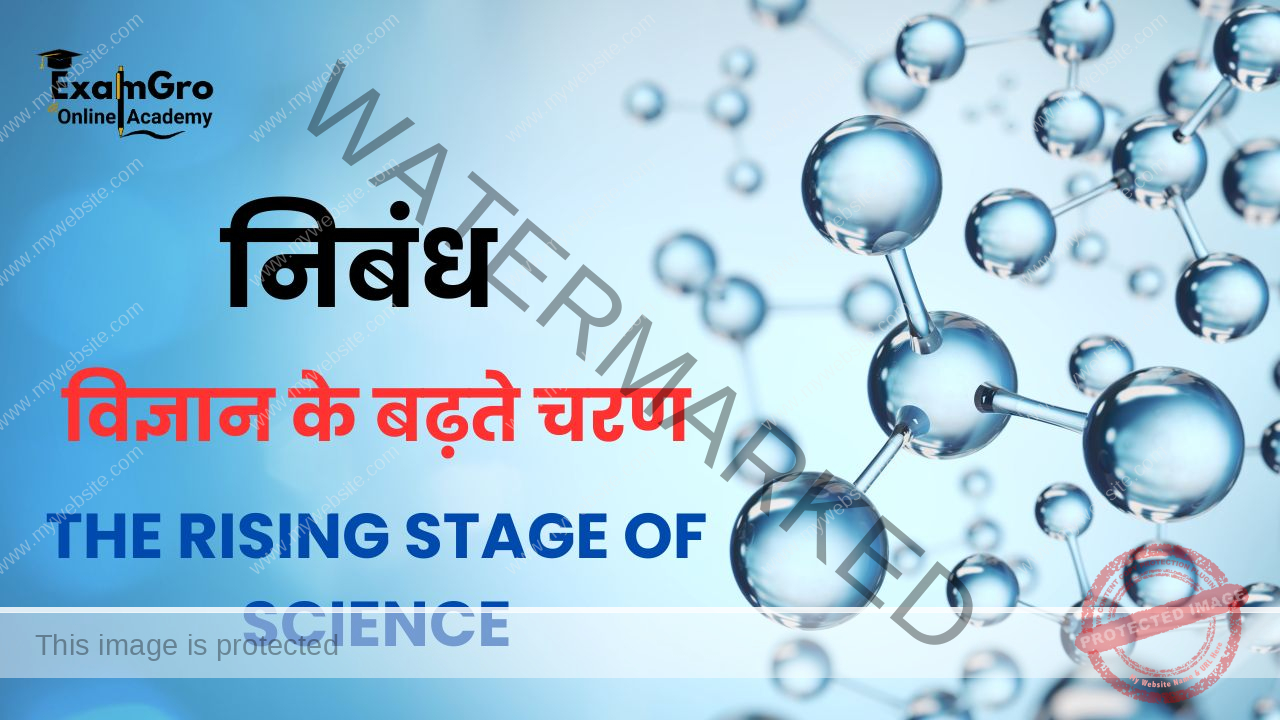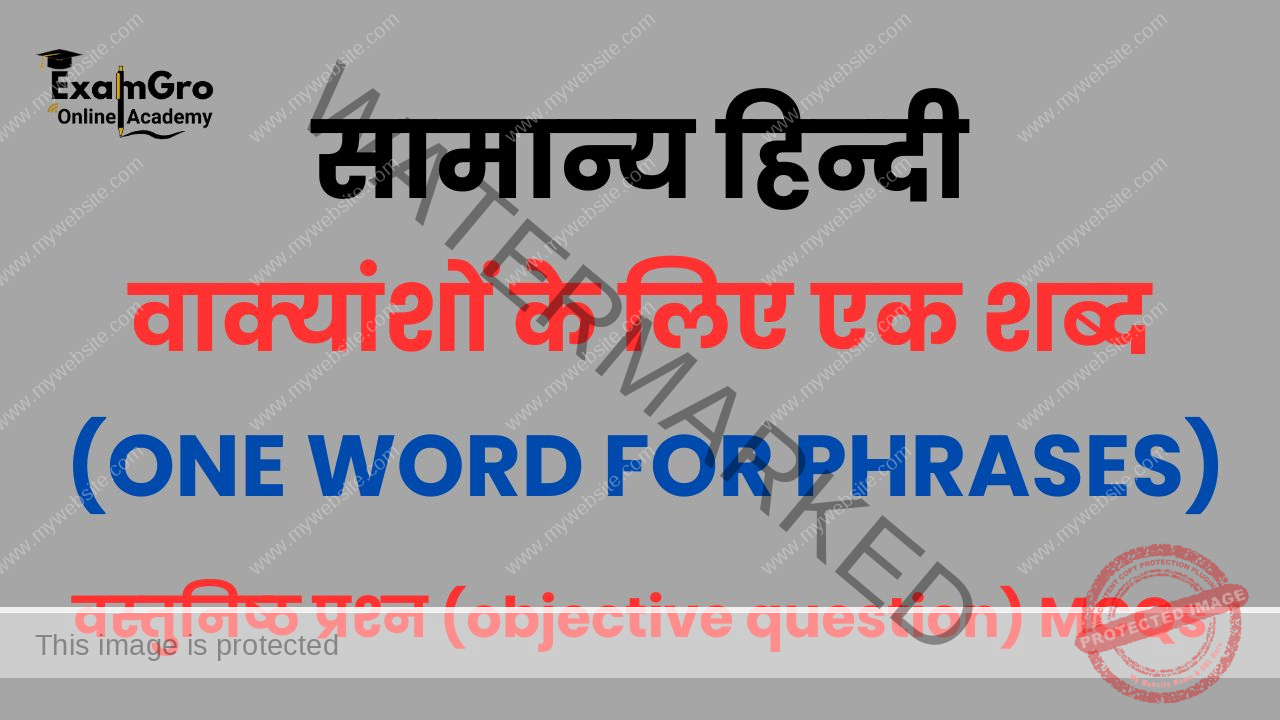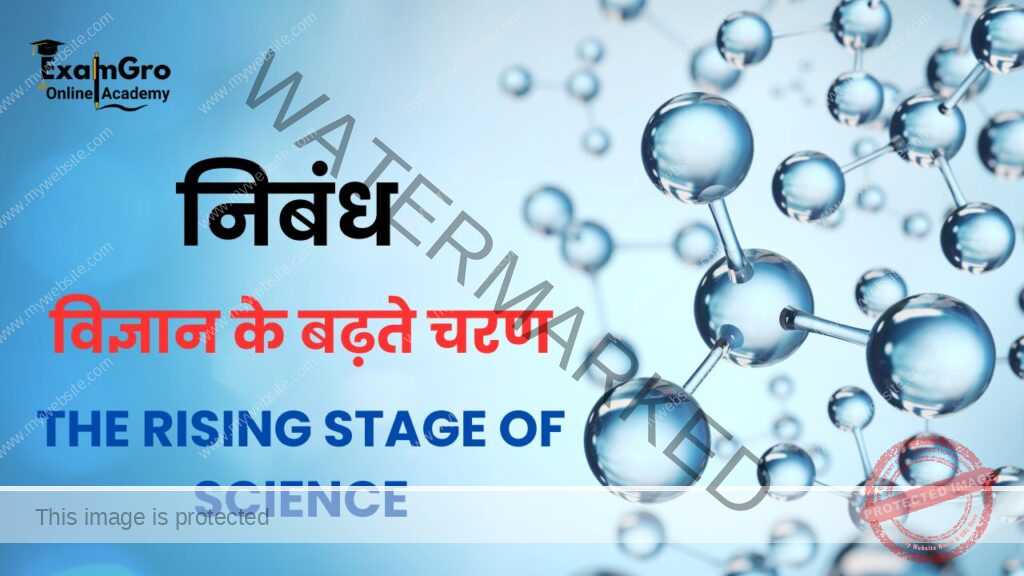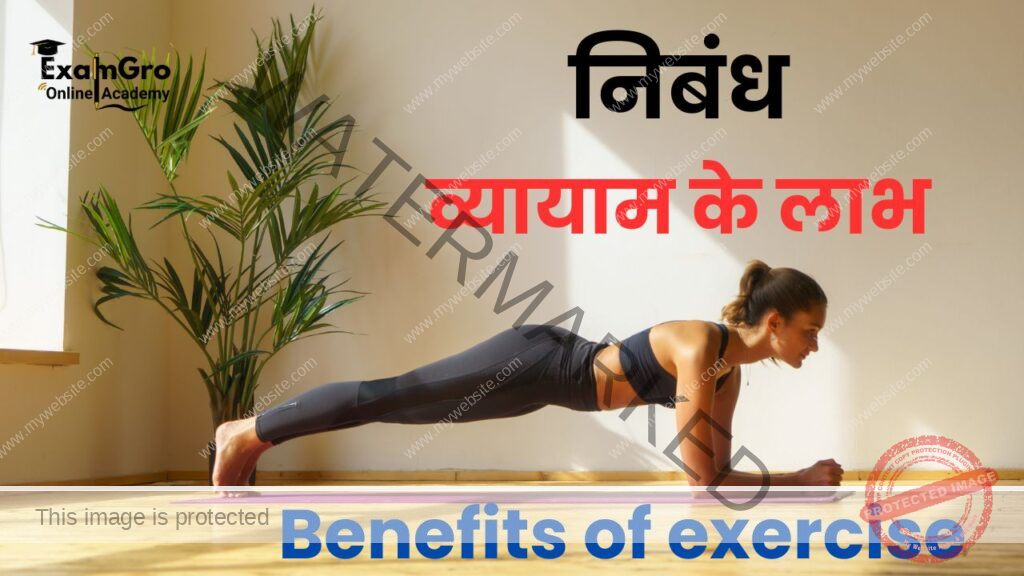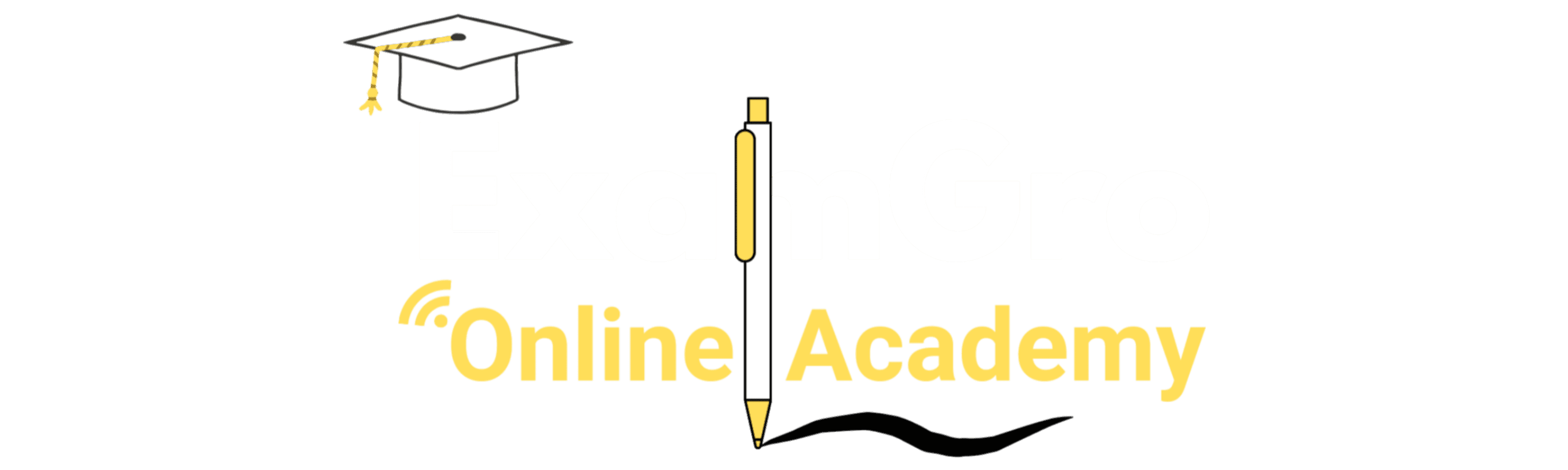पंचायती राज:- चौथी या पाँचवीं कक्षा में स्वर्गीय प्रेमचन्द की लिखी ‘पंच परमेश्वर’ नामक एक ज्ञानवर्द्धक और मनोरंजक कहानी पढ़ी थी ! पंचायत क्या होती है, वह आपसी झगड़ों या मामलों का निपटारा कैसे किया करती है, इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे यह सब पहली बार पता चल सका था। पंचायतों का महत्त्व भी तब में पहली बार ही जान सका था। इस कहानी को पढ़कर लगता है कि सन् 1915 के आस-पास जब यह कहानी लिखी गयी थी, तब इस देश में पंचायती राज चाहे न रहा हो, पर देहातों में पंचायतें अवश्य मौजूद रही होंगी। अपने छोटे-मोटे झगड़े निपटाने के लिए लोग उन्हीं के पास जाते होंगे। पंचायतों द्वारा दिये गये फैसलों से भी सन्तुष्ट होते होंगे ! जो हो, यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि कभी इस देश में पंचायती राज पूरी आन-बान के साथ चला करता था । उसे छोटे-बड़े हर प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार भी रहता था । यहाँ तक कि युद्ध और सन्धि करने जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णय भी पंचायतें किया करती थीं !
पंचायती राज
पंचायत को हम न्यायपालिका की छोटी-से-छोटी इकाई कह सकते हैं ! इसमें अपने कार्य-क्षेत्र के अनुसार ग्राम-क्षेत्र के चुने हुए लोग पंच के रूप में रहा करते हैं। ‘पंच’ का अर्थ पाँच होता है, जिसका तात्पर्य है पाँच जनों का संघ ! उनका मेल पंचायत कहलाता है । उसके द्वारा चलायी गयी व्यवस्था और प्रणाली को पंचायती राज कहा जाता है। पहले पंचों का चुनाव कैसे होता होगा, इस बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु लगता यही है कि देहातों की जनता ही मिलकर पंचों का चुनाव करती होगी। जनसंख्या के आधार पर ही उन पंचों की संख्या भी रहती होगी ! उन्हीं में से एक सरपंच अर्थात् पंचों में प्रमुख चुन लिया जाता होगा ! फिर वही सब मिलकर ग्राम स्तर की राज्य इकाई की सब प्रकार की व्यवस्था चलाते होंगे । न्याय-निर्णय करने का अधिकार भी उसी के पास होगा । इस प्रकार वह सब प्रकार से समर्थ, अपने-आप में पूर्ण एक व्यवस्था रही होगी। इसी कारण उसे पंचायती राज कहा जाता होगा ।
पंचायती राज की कल्पना वास्तव में गणतंत्र की ही देन मानी जाती है । राजशाही या विशुद्ध तानाशाही व्यवस्था में पंचायती राज की कल्पना सार्थक नहीं हो सकती ! भारत के प्राचीन इतिहास में मालव गणराज्य, मद्र गणराज्य, क्षुद्रक गणराज्य जैसे राज्यों और उनकी व्यवस्थाओं का वर्णन आता है । लगता है, राजसत्ता और व्यवस्था में आम जन या सामान्य-से- सामान्य जन को शामिल करने की भावना ने ही पंचायती राज की व्यवस्था को उपरोक्त गणराज्यों में अपनाया गया होगा। इनकी सफलता के कारण, इनसे प्रभावित होकर शेष राज्यों की ग्रामीण व्यवस्था के लिए इसे अपना लिया होगा ! प्राचीन भारत की शासन-व्यवस्था में ग्राम-पंचायतों और पंचायती राज का अपना निश्चित महत्त्व रहा है, तब के इतिहास एवं व्यवस्था सम्बन्धी ग्रन्थों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है । मध्यकाल में तो यह व्यवस्था रही ही, लगता है कि आधुनिक काल, बल्कि बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक दो दशकों तक भी इसका महत्त्व बना रहा। बाद में अंग्रेजी राज की नीतियों और स्वतंत्रता-आन्दोलनों के बढ़ते प्रभाव में इनका योगदान देखकर विदेशी शासक वर्ग ने प्रत्यक्ष रूप से इस पंचायती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यद्यपि देहातियों के मनों, आपसी व्यवहारों में इसके प्रति निष्ठा का भाव बना रहा !
स्वतंत्रता – प्राप्ति के बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार का ध्यान एक बार फिर इस व्यवस्था को दृढ़ करने की ओर गया। सन् 1950 में जब स्वतंत्र भारत का अपना संविधान बनकर लागू हो गया, उसमें भारत को जनतंत्र या गणतंत्र घोषित कर दिया गया, तभी दूर-दराज के आम आदमी यानि देहाती आदमी को भी शासन व्यवस्था का अंग और भागीदार बनाने के लिए पंचायती राज की कल्पना दोबारा सामने आयी । आम उपभोक्ता वस्तुओं – केरोसिन, चीनी-चावल आदि की किल्लत और भेद-भावपूर्ण वितरण प्रणाली ने भी पंचायतों की आवश्यकता को उजागर किया । अर्थात् देहातों में पंचायतों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को वितरण करने का मार्ग समझाया गया ! दूसरे, पहले की तरह ही लोग अदालतों की तरफ न भाग सामान्य झगड़े वहीं निपटा लें, इस बात ने भी पंचायती राज व्यवस्था को आवश्यक बना दिया। सो स्वतंत्र भारत में पंचायतों, एवं पंचायती राज व्यवस्था को एक बार फिर जीवित किया गया। आरम्भ के कुछ वर्षों तक यह व्यवस्था ठीक चलती रही । लोग न्याय और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ ठीक प्रकार से पाते रहे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे देश के अन्य क्षेत्रों में, उच्च राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ता गया, पंचायतें भी उसके प्रभाव से बच न पायीं। स्वार्थों की सिद्धि और अधिकार की भूख मिटाने का अड्डा पंचायतों को भी बना दिया गया। यहाँ भी भाई-भतीजावाद, जिसकी लाठी उसकी भैंस’ और ‘समर्थ को नहीं दोष गोसाईं ‘ जैसे सिद्धान्त लागू हो गये । समर्थ स्वार्थी तत्त्व अन्य क्षेत्रों के समान इस क्षेत्र में भी प्रभावी होते गये। फलस्वरूप इनका असली मकसद और मुद्दा पीछे छूटता गया । केवल स्वार्थ पूर्ति और शक्ति-परीक्षण के मुद्दे सामने आते गये। फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में जो दुर्दशा जन-उपयोगी अन्य संस्थाओं और व्यवस्थाओं की हुई, आज उससे भी कहीं बदतर पंचायतों और पंचायती राज व्यवस्था की हो रही है । आज इनका वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक स्वरूप लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। रह गया है मात्र ढाँचा, उसका मांस भी सत्ता और धन के भूखे गिद्ध, कौए, गीदड़ नोचकर खा चबा जाना चाहते हैं !
इसे भी पढें:- भारत की स्वतंत्रता के चवालीस वर्ष-निबंध
पहले जब पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव हुआ करते थे, तब स्वार्थहीन और सच्चे जन-सेवक लोग चुनकर आ जाते थे। उनके कारण सब ठीक-ठाक चला करता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे संसद और विधान परिषदों के चुनावों में धन-बल, असामाजिक तत्त्वों के बल का प्रभाव बढ़ने लगा, वैसे ही यहाँ भी वही सब होने लगा। गाँव के बड़े जमींदार, महाजन और पण्डित आदि आपसी मिलीभगत से पंचायतों पर अधिकार करने लगे। स्वार्थहीन और सच्चे समाज-सेवकों ने यदि पंचायतों में चुनाव के द्वारा आने का प्रयत्न भी किया, तो गुण्डों की सहायता से उन्हें हटा दिया गया। कइयों को तो प्राण तक भी गँवाने पड़े। धीरे-धीरे अनेक प्रकार के डर के कारण अच्छे लोगों ने पंचायतों से दूर रहना ही उचित समझा। सो अब न्याय-अन्याय का निर्णय तो लाठी के दबाव से होने ही लगा, उपभोक्ता वस्तुएँ भी काला बाज़ार में और उनके मुनाफे पंचों के घर पहुँचने लगे। पंचों ने मिलकर चरागाहों की भूमि या तो बेच दी या अपने अधिकार में कर ली। पंचायत की भूमि के साथ भी ऐसा ही किया गया और आज भी घड़ल्ले से किया जा रहा है। गाँवों का वातावरण आज जो इतना गन्दा, न रहने के योग्य हो गया है, उसका मुख्य कारण परम्परा से चली आ रही पंचायती राज-व्यवस्था का चरमरा जाना ही माना जाता है ।
इस प्रकार कुल मिलाकर पंचायतें और पंचायती राज व्यवस्था भारत की अन्य समस्त व्यवस्थाओं के समान ही आम आदमी के लिए व्यर्थ होकर रह गयी है। पंचायत घर भ्रष्टाचार के अड्डे और व्यवस्था बेचारे आम आदमी को लूटने, एकदम नंगा करके रख देने का साधन बन गयी है। स्वर्गीय प्रेमचंद ने अपनी कहानी ‘पंच परमेश्वर’ के पंचों में जिस परमेश्वर का वास देखा था, वह फिर कभी दिखायी दे पायेगा— नहीं, अब कभी भी दिखायी दे पाना सम्भव नहीं लगता !